“रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं क़ायल
जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है।”
यह पंक्ति है महशूर शायर मिर्जा गालिब के जिनका हाल में ही 27 दिसंबर हो जन्मदिवस मनाया गया है। इनका भौतिक जीवन काल तो 27 दिसंबर 1796 से 15 फरवरी 1869 तक रहा लेकिन इनकी रचनाएँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सच तो यह है कि उर्दू शायरी की बात बिना गालिब के पूर्ण हो ही नहीं सकती है। आम लोग जिस शायर को सबसे ज्यादा जानते हैं वह गालिब ही हैं।
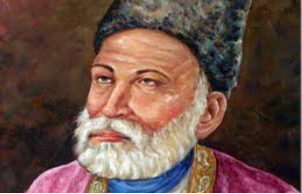
रचनाएँ
गालिब ने मात्र ग्यारह वर्ष की उम्र से उर्दू और फारसी में लिखना शुरू कर दिया। वह पद्य (काव्य) और गद्य दोनों रूपों में लिखते थे। लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध वे अपने गजलों और नज़मों के लिए हुए। पर उन्होने कसीदा, रुबाई, कीतआ, मर्सिया आदि शैली/विधा में भी लिखा।
उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है ‘दीवान-ए-गालिब’। उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित उनके पत्रों का संग्रह भी उर्दू भाषा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जाता है।
वह मुख्यतः प्रेम, विरह, दर्शन, रहस्यवाद आदि विषयों पर लिखते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि उनके विषयों के कारण नहीं बल्कि आम बोलचाल में आम अनुभवों की बात कहने की थी। वह स्वयं लिखते हैं
हैं और भी दुनिया में सुख़नवर बहुत अच्छे
कहते हैं कि ‘ग़ालिब’ का है अंदाज़-ए-बयाँ और
गालिब के विरासत
गालिब एक महान शायर तो थे ही लेकिन जिस समय वह हुए थे वह बहुत बड़े परिवर्तनो का दौर भी था। 1857 की क्रांति, मुग़ल साम्राज्य का पतन और अँग्रेजी राज्य का उत्थान सबका- उन्होने करीब से अनुभव किया। पुराने नाबावों और शाही लोगों और उनके साथ कलाकारों, कवियों आदि का पतन भी वह देख रहे थे।
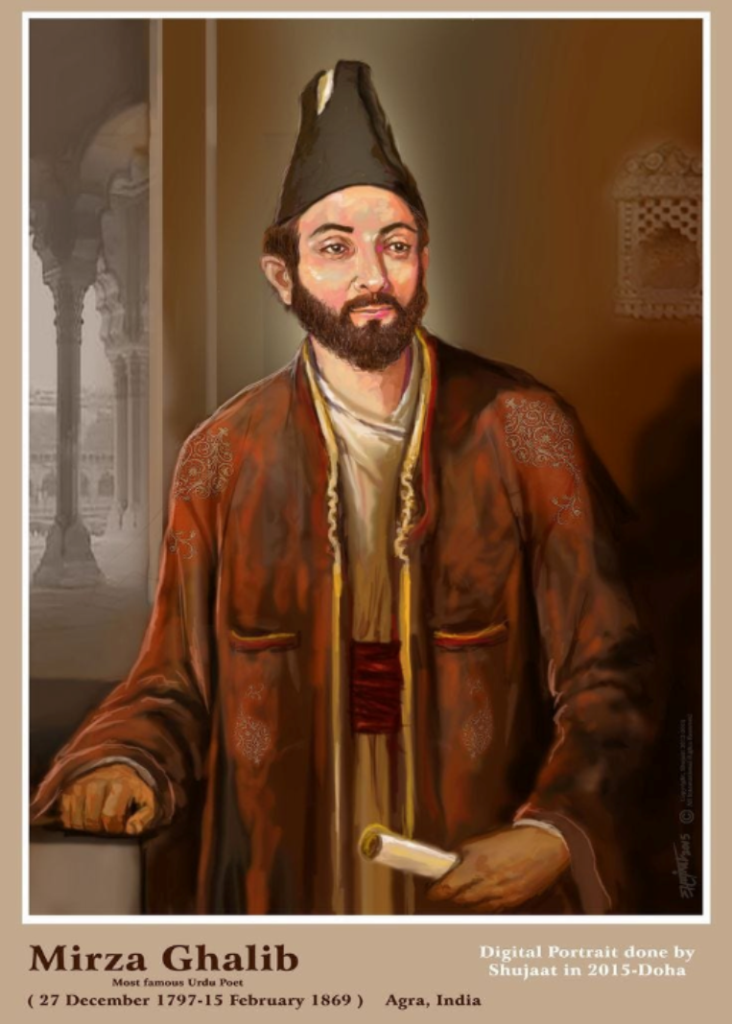
बहादुरशाह ज़फ़र, अल्ताफ हुसैन हाली, मिर्ज़ा दाग देहलवी, नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, शेख़ मुहम्मद इब्राहीम, जौक, मोमिन खान मोमिन, हकीम महमूद खान इत्यादि गालिब के समकालीन उर्दू के शायर थे। इन सबने उर्दू भाषा और शायरी को सम्मानजनक स्थान दिलाने में बहुत योगदान दिया है। लेकिन अपने अलग अंदाजे बयां के कारण गालिब उर्दू शायरी के एक ऐसे पर्याय बन गए जो किसी देश, काल या भाषा की सीमा से बंधे नहीं रहे। गालिब पर शोध करने वाले राल्फ़ रसल (Ralph Russell) तो कहते हैं ‘यदि गालिब अँग्रेजी भाषा में लिखते तो विश्व एवं इतिहास के महानतम कवि होते।’
गालिब उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर तो थे ही वे बहुत ही अच्छे पत्र लेखक भी थे। यद्यपि भारत (संयुक्त भारत) में फारसी भाषा को आम लोगों में हिन्दुस्तानी जबान के रूप में प्रयोग करने का श्रेय मीर तकी ‘मीर’ को दिया जाता है। पर इस जुबान को आम जीवन से जुड़े शायरी में ढ़ाल कर लोकप्रिय बनाया था मिर्जा गालिब ने। उर्दू शायरी ही नहीं, भाषा के लिए उनका योगदान भी सार्वकालिक है। उन्होने अपने जीवन काल में कई पत्र लिखे थे जो कि उनके निधन के बाद प्रकाशित हुए। ये पत्र भी उर्दू लेखन के बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं।
व्यक्तिगत जीवन
उनका वास्तविक नाम था मिर्जा असदुल्लाह बेग खान। लेकिन वह लिखते थे ‘गालिब’ और ‘असद’ के नाम से। इसीलिए वे प्रसिद्ध मिर्जा गालिब के नाम से हुए।
गालिब का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के आगरा में एक तुर्क परिवार में 27 दिसंबर 1796 को हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग और माता का नाम इज्जत उत निसा था। यह परिवार 1750 के आसपास अहमद शाह के शासनकाल में वर्तमान उज्बेकिस्तान के समरकन्द से आकर भारत में बस गया था। जब गालिब करीब पाँच वर्ष के थे तभी अलवर के युद्ध में उनके पिता की मृत्यु हो गई। माँ का निधन भी जल्दी ही हो गया। माता-पिता की मृत्यु के बाद चाचा ने उनका पालन पोषण किया था। उनके चाचा मिर्जा नसरुल्ला बेग खान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत सैन्य अधिकारी थे। चाचा की मृत्यु के बाद अँग्रेजी सरकार उनके परिवार को जो पेंशन देती थी, वही गालिब के गुजारे का जरिया था। उनके पिता और चाचा दोनों सैनिक थे लेकिन गालिब का मन इससे बिलकुल उल्टा शेरो-शायरी में रमता था। लेकिन उनके किसी औपचारिक शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है कहीं।
उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में उमराव बेगम से हुआ था। विवाह के बाद वह आगरा छोड़ कर दिल्ली में रहने लगें। यहीं वह कुछ दिनों तक मुगल बादशाह बहदुर शाह जफर द्वितीय के दरबारी शायर भी रहे। 1850 में बादशाह ने उन्हें ‘दबीर-उल-मुल्क’ और ‘नज्म-उद-दौला’ का खिताब दिया। दरबार में उनका रुतबा बढ़ ने लगा। उन्हें शहजादा मिर्जा फखरू का शिक्षक और मुगल दरबार का शाही इतिहासविद भी नियुक्त किया गया। उन्हें ‘मिर्जा निशा’ का खिताब भी मिला।
1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर म्यांमार (तात्कालीन बर्मा) भेज द दिया गया। पर गालिब दिल्ली में ही रहते रहे। यहीं 15 फरवरी 1869 को उनका निधन हुआ।
शराब, भोजन, हुक्के और शतरंज के शौकीन गालिब के अंतिम दिन आर्थिक और मानसिक कष्ट में गुजरे थे। बहादुर शाह बाद में स्वयं अंग्रेजों के पेंशन पर निर्भर हो गए थे। मुगल शासन समाप्त होने के बाद अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें दरबार से मिलने वाला वजीफा बंद कर दिया। अब वे उस पेंशन पर निर्भर थे जो उनके चाचा की मृत्यु के बाद उनके परिवार को अंग्रेज़ सरकार से मिलता था। यह पेंशन अनियमित थी। बाद में इसे भी बंद कर दिया गया। इसे फिर से शुरू करवाने के लिए उन्हें कई बार कोलकाता (तात्कालिक कलकता) भी जाना पड़ता था। इसका जिक्र उनके कुछ शायरी में भी है। पर यह पेंशन शुरू नहीं हो पायी।
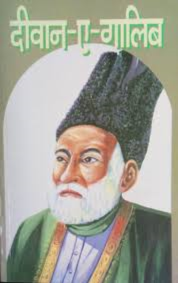
आर्थिक तंगी के अलावा मानसिक कष्ट भी सहने पड़े थे उन्हें। उनके सात बच्चों की मृत्यु उनके सामने ही हो गई। 1857 के खून खराबे में उन्होने अपने छोटे भाई मिर्जा युसुफ अली सहित कई करीबियों को खोया। मुगल बादशाह और शाहजादों का अंत देखा। इन सबका का उनके मानसिक और शारीरिक स्वस्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा।
1857 के विद्रोह में कई लोगों को खोने के बाद उनकी मानसिक तकलीफ का आभास 8 सितंबर 1858 को उनके मित्र हकीम अजहददौला नजफखा को लिखे गए एक पत्र से पता चलता है ‘वल्लाह, दुआ मांगता हूं कि अब इन अहिब्बा (प्रिय) में से कोई न मरे, क्या मानें के जब मैं मरूं तो मेरी याद करने वाला, मुझ पर रोने वाला भी तो कोई हो।’
मुसलमान होने के बावजूद शराब पीने के शौकीन होने के कारण वह अपने को ‘आधा मुसलमान’ कहते थे। उन्होने कभी रोजा नहीं रखा था। 1847 में जुआ खेलने के कारण उन्हें अग्रेज़ सरकार ने जेल में भी डाल दिया था। इन सब कारणों से उनकी आलोचना भी की जाती थी।
पर अपनी हाजिर जवाबी और नज़मों के कारण उनकी लोकप्रियता हर वर्ग में उस समय भी थी और आज भी है। उनके ऐसे शेरों के बिना आज भी हर महफिल शायद अधूरी सी लगती है
वो आए घर में हमारे, खुदा की क़ुदरत हैं!
कभी हम उमको, कभी अपने घर को देखते हैं
हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है
तुम्हीं कहो कि ये अंदाज़-ए-गुफ़्तगू क्या है
*****

Interesting read! Seeing platforms like big bunny apk cater specifically to the Philippine market with GCash & PayMaya is smart. Security is key though – always verify those new sites & 2FA!